राजकोषीय घाटा क्या है? जीडीपी, जीएसटी का क्या मतलब है? बजट के 10 शब्दों का मतलब समझें।
1 min read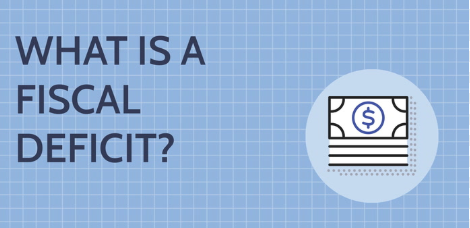
 कृपया इस न्यूज को शेयर करें कृपया इस न्यूज को शेयर करें   |








कई लोगों को बजट बनाना जटिल लगता है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि बहुत से लोग इसमें प्रयुक्त शब्दों को समझ नहीं पाते। तो आइए बजट में प्रयुक्त 10 शब्दों और आम भाषा में उनके अर्थ को समझते हैं।
जब बजट का जिक्र होता है तो कई लोगों के मन भटक जाते हैं। प्रायः बजट के तकनीकी पहलू आम जनता को समझ में नहीं आते। बहुत से लोग शब्दों को नहीं समझते, विशेषकर वित्तीय मामलों से संबंधित शब्दों को। इसीलिए, इस वर्ष के बजट, यानी 2025 के बजट से पहले, हम यह जानने जा रहे हैं कि बजट का नियमित विश्लेषण और प्रस्तुति करते समय किन शब्दों का उपयोग किया जाता है और उनका क्या अर्थ होता है।
केंद्रीय बजट
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, केंद्रीय बजट की परिभाषा इस प्रकार है: केंद्रीय बजट सरकार की प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। यह अनुमान किसी विशेष वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो बजट एक विशिष्ट समयावधि के लिए वित्तीय योजना है। केंद्रीय बजट विभिन्न परियोजनाओं और एजेंसियों को धन आवंटित करने की सरकार की योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। चूंकि कर भारत सरकार के लिए राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, इसलिए केंद्रीय बजट में कर की दरों और नियमों में किसी भी परिवर्तन को निर्दिष्ट किया जाता है।
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) बजट के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी देश में उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है। अधिकांश देशों में, आर्थिक विकास को मापने का मानक सकल घरेलू उत्पाद है। सकल घरेलू उत्पाद की गणना वार्षिक या त्रैमासिक आधार पर की जा सकती है। भारत में, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से जानकारी एकत्र करके देश के सकल घरेलू उत्पाद की गणना करता है। भारत सरकार तिमाही आधार पर जीडीपी के आंकड़े जारी करती है। अंतिम आंकड़े 31 मई को जारी किये जायेंगे।
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर
कर सरकारी राजस्व का प्राथमिक स्रोत हैं। भारत में दो प्रकार के कर लगाए जाते हैं। एक है प्रत्यक्ष कर और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो किसी व्यक्ति द्वारा सीधे सरकार को दिया जाता है। इसमें आयकर और कॉर्पोरेट कर शामिल हैं। दूसरी ओर, अप्रत्यक्ष कर वह है जब किसी व्यक्ति या संगठन के माध्यम से सरकार को कर का भुगतान किया जाता है। अप्रत्यक्ष कर का एक सरल उदाहरण जीएसटी है। जब आप कोई उत्पाद/सेवा खरीदते हैं, तो विक्रेता को उसकी बिक्री पर सरकार को कर का भुगतान करना होता है। हालाँकि, उन्हें जीएसटी के माध्यम से ग्राहकों से कर वसूलने की अनुमति है। यह राशि अंततः सरकार के पास जमा कर दी जाती है। इसलिए, विक्रेता ग्राहकों से कर वसूलते हैं, जिससे वे अप्रत्यक्ष करदाता बन जाते हैं।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)
जीएसटी, या वस्तु एवं सेवा कर, भारत में बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुओं/सेवाओं पर लगाया जाता है। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, जिसमें कर का भुगतान उपभोक्ता करता है, लेकिन राशि व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा सरकार को भेज दी जाती है। जीएसटी से सरकार का राजस्व बढ़ता है।
सीमा शुल्क
जब कोई व्यक्ति भारत में वस्तुओं का आयात या निर्यात करता है, तो सरकार लेनदेन राशि पर कर लगाती है। यद्यपि इस राशि के भुगतान का वित्तीय भार आयातक या निर्यातक पर पड़ता है, लेकिन आमतौर पर इसका भार उपभोक्ता को उठाना पड़ता है। इसलिए यह भी अप्रत्यक्ष कर का एक रूप है।
राजकोषीय घाटा
राजकोषीय का अर्थ है सरकारी राजस्व। घाटे का मतलब है सरकारी राजस्व में राजकोषीय कमी! सरल शब्दों में, इसका अर्थ है सरकार के व्यय से संबंधित उधार न ली गई प्राप्तियों (आय) में घाटा या कमी। यदि व्यय प्राप्तियों (गैर-उधार) से अधिक है, तो कुल व्यय और सरकार की कुल गैर-उधार प्राप्तियों के बीच का अंतर उसका राजकोषीय घाटा है। इसे आमतौर पर किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
पूंजीगत बजट
पूंजी बजट में पूंजी प्राप्तियां और पूंजी व्यय शामिल होते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विनिवेश, जनता से ऋण, विदेशी सरकारों और संस्थाओं से ऋण, आरबीआई से ऋण, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और अन्य पक्षों से ऋण की वसूली आदि शामिल हैं। जबकि पूंजीगत व्यय में स्वास्थ्य सुविधाओं, मशीनरी, सड़क, भूमि, भवन आदि के विकास के लिए सरकार द्वारा किया गया व्यय तथा केंद्र सरकार द्वारा राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, सरकारी कंपनियों, निगमों व अन्य पक्षों को दिए गए ऋण शामिल होते हैं।
राजकोषीय नीति
जब कोई देश बजट की घोषणा करता है तो उसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि सरकार आयकर की दर में परिवर्तन करती है, तो इससे लोगों की प्रयोज्य आय प्रभावित होगी तथा उनकी क्रय शक्ति भी प्रभावित होगी। इससे व्यवसायों के साथ-साथ सरकार के कर राजस्व पर भी असर पड़ता है। इसलिए, सरकार अपनी व्यय और कर नीतियों का उपयोग इस तरह से करती है कि उनका देश की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। इन नीतिगत निर्णयों को सरकार की राजकोषीय नीति कहा जाता है। बजट प्रायः राजकोषीय नीति का सूचक होता है।
मौद्रिक नीति
अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था की वृद्धि को प्रभावित करता है। इसलिए, सरकार वांछित विकास सुनिश्चित करने के लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति या तरलता पर नज़र रखती है। यह कार्य देश के केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। भारत में बैंकों का केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नाम से जाना जाता है। मौद्रिक नीति, आरबीआई का कार्य है जो सतत विकास प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करता है।
मुद्रा स्फ़ीति
यह बताने के कई तरीके हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है। यह अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि है। मुद्रा की क्षमता भी कम हो जाती है। समय के साथ मुद्रा का मूल्य भी घटता है। सरल शब्दों में कहें तो आज आपके पास एक हजार रुपये हैं जिनसे आप कुछ वस्तुएं/सेवाएं खरीद सकते हैं। हालाँकि, आज से दस साल बाद, आपको आज के बराबर पैसे में उतनी ही मात्रा में वस्तुएँ और सेवाएँ नहीं मिलेंगी। इसे मुद्रा के मूल्य में कमी कहा जाता है।
About The Author
|
Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें |
Advertising Space














Recent Comments